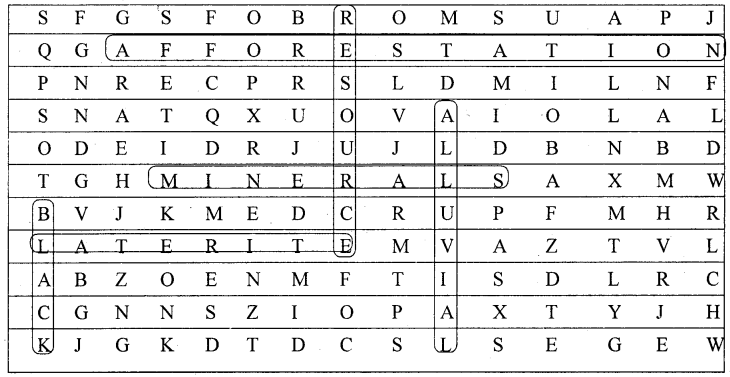Haryana State Board HBSE 10th Class Social Science Solutions History Chapter 3 भारत में राष्ट्रवाद Textbook Exercise Questions and Answers.
Haryana Board 10th Class Social Science Solutions History Chapter 3 भारत में राष्ट्रवाद
HBSE 10th Class History भारत में राष्ट्रवाद Textbook Questions and Answers
1. व्याख्या करें
(क) उपनिवेशों में राष्ट्रवाद के प्रक्रिया उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन से जुड़ी हुई क्यों थी।
उत्तर-
‘राष्टीयता’ या ‘राष्ट्रवाद’ एकता की वह शक्तिशाली भावना है जो लोग तब अनुभव करते है जब वे एक जैसी राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक अवस्थाओं में रहते है, जब वे एक जैसी आंकाक्षायें रखते हैं और जब वे विशेष भू- भाग में एक विशेष राजनितिक व्यवस्था के अधीन रहते हैं और एक नियमों का पालन करते हैं। राष्टीयता एक ऐसी भावना है जो विश्व के इतिहास में मध्य-युग के पश्चात् दृष्टिगोचर हुई। यह उन्हीं सामाजिक एवं आर्थिक कारणों का परिणाम है जिन्होंने सामंतवाद का अन्त किया था।
साधारणतया यह देखा गया है कि उपनिवेशों में राष्ट्रवाद के उदय की प्रक्रिया उपनिवेशवाद-विरोधी आन्दोलन से जुड़ी हुई होती है। उपनिवेशवाद शोषण पर आधारित होता है। उपनिवेशवाद शोषण पर आधारित होता है इसलिये समाज के सभी प्रकार के लोग इस लूट-खसूट से इतने तंग आ जाते है कि वे विदेशी उपनिवेशवाद को समाप्त करने और अपने देश को स्वतन्त्र कराने का दृढ़ संकल्प कर लेते हैं। बहुत बार शोषण और अन्याय ही बड़े-बड़े और आंदोलनों का कारण बनता है।
अंग्रेज़ी उपनिवेशवादियों ने भारत को ऐसे लूटा कि हर वर्ष पड़ने वाले अकाल की लपेट में आने लगे और उनके मन में अत्याचारी सरकार के विरुद्ध आक्रोश के भाव जागृत होने लगे। ‘मरता क्या न करता’ वाली कहावत के अनुसार लोगों को यह एहसास हो गया कि वे जब तक अपने देश को स्वतन्त्र नहीं करा लेंगे उनके दुखों को तब तक अंत नहीं हो सकता।
जीवन के हर क्षेत्र में उपनिवेशवादियों द्वारा झूठ-फरेब, नीच और अन्यायपूर्ण हथकंडे अपनाने के कारण वे जनता में शीघ्र ही बदनाम हो गए। अब वे जान चुके थे कि जब तक वे अपने देश को स्वतन्त्र नहीं करा लेते वे चैन की नींद सो नहीं सकते। इस नरक से निकलने का एक ही तरीका है कि उपनिवेशवाद को खत्म किया जाए और देश को स्वतन्त्र कराया जाए।
(ख) पहले विश्व युद्ध ने भारत में राष्टीय आंदोलन के विकास में किस प्रकार योगदान दिया।
उत्तर-
(1) प्रथम विश्व युद्ध लाए गए आर्थिक संकट के कारण भारतीयों में रोष और विरोध की भावना-ज्योंही 1914 ई. में यह युद्ध में शुरु हुआ भारत में उथल-पुथल पैदा हो गई। पहले तो अंग्रेजों ने भारतीयों से पूछे बिना युद्ध में भारत को भी एक पार्टी बना दिया और दूसरे, भारत के संसाधनों का धड़ाधड़ प्रयोग ब्रिटिश सरकार अपनी विदेशी हितों की पूर्ति के लिए कर रही थी। इससे चीजों के मूल्य बढ़ गए और लोगों के लिये जीना कठिन हो गया। इसीलिए भारतीयों में अंग्रेजों के प्रति बड़ा रोष पैदा हुआ।
(2) राजनीतिक गतिविधियों का तेज़ हो जाना और होमरुल आन्दोलनों का ज़ोर पकड़ना–प्रथम विश्व युद्ध में फंसे देखकर भारतीयों ने अंग्रेजों से कुछ अधिकार प्राप्त करने के प्रयत्न किए। श्रीमती एनी बेसेंट 1914 ईद में कांग्रेस में शामिल हुई थीं। दो वर्ष बाद गंगाधर तिलक के साथ मिलकर उन्होंने होमरुल आंदोलन की नींव रखी और होमरुल लीग की स्थापना की जिसका लक्ष्य भारतीयों के लिए होमरुल या स्वराजय प्राप्त करना था। किन्तु ब्रिटिश सरकार इसके लिए तैयार नहीं थी इसलिये उसने एनी बेसेंट को गिरफ्तार कर लिया और इस आंदोलन को कुचलने के लिए दमनचक्र चलाया।
(3) मुस्लिम लींग और कांग्रेस का एक-दूसरे के निकट आना और इस प्रकार राष्ट्रीयता को बल मिलना-यद्यपि मुस्लिम लींग अंग्रेजी सरकार की बांदी थी तथापि प्रथम महायुद्ध की घटनाओं के कारण इसे कांग्रेस के समीप आना पड़ा। तुर्की ने प्रथम महायुद्ध में मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध जर्मनी का साथ दिया था। युद्ध की समाप्ति पर अंग्रेजों ने उसके साथ कठोर व्यवहार किया जिससे भारत के मुसलमान, विशेष रुप से मुस्लिम लींग, – ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध हो गए कांग्रेस के साथ 1916 ईद में उन्होने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए।
(4) नरमदल और गरमदल में पुनः मैत्री स्थापित होना और स्वतन्त्रता संग्राम को मजबूती से मिलना-सरकार की दमन नीति के कारण नर्मदल और गर्मदल के नेताओं में 1916 ई. में पुनः मेल-मिलाप हो गया।
(5) प्रथम विश्व युद्ध द्वारा फैलाए गए रोष के कारण वातावरण में गांधी जी द्वारा राष्ट्रीयता की बागडोर संभालना आसान हो जाना-प्रथम महायुद्ध के दौरान ही गांधी जी का भारत के राष्ट्रवादी आंदोलन के नेता के रूप में उदय हुआ।
(ग) भारत के लोग रोलट एक्ट के विरोध में क्यों थे।
उत्तर-
रौलट ऐक्ट, 1919 ई.-1919 ई. के गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया ऐक्ट में दी गई रियासतों से काँग्रेस असन्तुष्ट थी और समस्त भारत में निराशा का वातावरण छाया हुआ था। सरकार को डर था कि अवश्य कोई नया आन्दोलन प्रारम्भ होगा। इस ऐक्ट के अनुसार सरकार की किसी भी व्यक्ति को बिना अभियोग चलाए अनिश्चित समय के लिए बन्द कर सकती थी और उसे अपील, दलील या वकील करने का कोई अधिकार नहीं था।
इस ऐक्ट के प्रति भारतीय प्रतिक्रिया और सरकारी दमन-इस ऐक्ट के विरुद्ध सभी भारतीय एक-साथ खड़े हो गए। उन्होंने इसे ‘काले बिल का’ नाम का नाम दिया। यह राष्ट्रीय सम्मान पर ऐसा धब्बा था जिसे भारतीयों के लिए सहना बड़ा कठिन था। ऐसे कठिन समय में महात्मा गाँधी ने राष्ट्रीय आन्दोलन की बागडोर सम्भाली और इसे नवीन कार्यक्रम और कार्यविधि प्रदान की। उन्होंने इस ऐक्ट के विरुद्ध सत्य और अहिंसा के आधार पर सत्याग्रह आन्दोलन शुरु किया। दिल्ली में एक भीड़ पर पुलिस ने गोली दी जिसमें पाँच व्यक्ति मारे गए और 20 घायल हुए। इसके विरोध में बड़े-बड़े शहरों में हड़ताले हुई और दुकानें बन्द कर दल गयीं। अनेक लोगों को सरकार ने पकड़ कर जेल में डाल दिया। महात्मा गाँधी ने भी जब वास्तविक स्थिति का अमययन करने के लिए दिल्ली और पंजाब की ओर जाने का प्रयत्न किया तो उन्हें भी पकड़ लिया गया।
इस प्रकार ऐक्ट ने भारत की राजनीति में उनर भर दी अंग्रजी सरकार और भारतीयों में टकराव का वातावरण पैदा कर दिया।
(घ) गांधीजी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला क्यों लिया।
उत्तर-
महात्मा गांधी ने असहयोग आन्दोलन को क्यों वापस ले लिया-असहयोग आन्दोलन अपने पूरे जोरों पर चल रहा था जब महात्मा गांधी ने 1922 ई. को उसे वापस ले लिया। इस आंदोलन के वापिस लिये जाने के कारण थे जिनमें से मुख्य निम्नलिखित है:
(1) महात्मा गांधी अहिंसा और शांति के पूर्ण समर्थक थे – इसलिए जब उन्हें यह सूचना मिली कि उत्तेजित भीड़ ने चौरी-चौरा के पुलिस थाने को आग लगा कर 22 सिपाहियों की हत्या कर डाली है तो वह परेशान हो उठे। उन्हें अब विश्वास न रहा कि वे लोगो को शान्त रख सकेंगे। ऐसे में उन्होंने असहयोग आन्दोलन को वापिस ले लेना ही उचित समझा।
(2) दूसरे वे सोचने लगे कि यदि लोग हिसंक को जायेंगे तो अंग्रेजी सरकार भी उत्तेजित हो उठेगी और आंतक का राज्य स्थापित हो जायेगा और अनेक निर्दोष लोग मारे जायेंगे। महात्मा गांधी जलियाँवाला बाग जैसे हत्याकांड की पुनरावृति नहीं करना चाहते थे इसलिए 1922 ई. में उन्होंने असहयोग आंदोलन वापिस ले लिया।
प्रश्न 2.
सत्याग्रह के विचार का क्या मतलब है?
उत्तर-
गाँधी जी ने सत्याग्रह के विचार के संदर्भ में चार बिन्दु निम्नलिखित है:
(1) सत्याग्रह सच्चाई और अहिंसा का एक ढंग है जिसे अपनाकर महात्मा गान्धी ने दक्षिण अफ्रीका की नस्लभेदी सरकार से सफलतापूर्वक लोहा लिया था बाद में यही पद्धति उन्होंने भारत की ब्रिटिश सरकार के अन्यायपूर्ण कार्यो का विरोध करने में अपनाई।
(2) यदि आपका उद्देश्य सच्चा और न्यायपूर्ण है तो आपको अन्त में सफलता अवश्य मिलेगी, ऐसा महात्मा गाँधी का विचार था।
(3) प्रतिरोध की भावना या आक्रमक्ता का सहारा लिये बिना सत्याग्रही केवल अहिंसा के सहारे अपने संघर्ष में सफल हो सकता है।
(4) बाद में सत्याग्रह के इसी सिद्धान्त का प्रयोग उन्होंने अनेक स्थानों पर किया जैसे 1916 में बिहार में चंपारन इलाके में दमनकारी बागान मालिकों के विरुद्ध किसानों को बचाने में,1917 ई. में गुजरात के खेड़ा जिले के किसानो को फसल खराब हो जाने के कारण सरकारी करों से बचाने में और 1918 में गुजरात के अहमदाबाद के सूती कपड़ा के कारखानों के मजदूरों को उचित वेतन दिलाने आदि में किया, परन्तु उन्हें हर बार सफलता प्राप्त हुई।
न्याय और सच्चाई पर आधारित सत्याग्रह का सिद्धान्त बाद में कांग्रेस के संघर्ष का मूल मंत्र बन गया।
प्रश्न 3.
निम्नलिखित पर अख़बार के लिए रिर्पोट लिखें
(क) जलियाँवाला बाग हत्याकांड
उत्तर-
जलियाँवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल, 1919 ई. -1918 ई. में प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया और उसके साथ ही भारत में होने वाली वस्तुओं की मांग भी बहुत कम हो गई जिससे किसान वर्ग (Peasants) को बहुत हानि हुई। बेकारी भी बहुत बढ़ गई, क्योंकि युद्ध समाप्त होने पर कइयों को नौकरी से छुट्टी मिल गई। जब चीजों की माँग कम हो गयी तो भारतीय व्यापारियों को भी बहुत कठिनाइयाँ उठानी पड़ी। जमीदारों का भी बहुत बुरा हाल था, क्योंकि किसानों से उन्हें लगान तो. मिल रहा था लेकिन सरकार उनसें पूरा लगान मा!गती थी। संक्षेप में प्रत्येक व्यक्ति बड़ा परेशान था। उधर जनवरी 1919 ई. को अंग्रेजी सरकार ने रौलट ऐक्ट पास करके लोगो में और भी रोष पैदा कर दिया। उधर महात्मा गाँधी ने इसके विरुद्ध सत्याग्रह प्रारम्भ कर दिया। सारे देश में हड़तालें होने लगीं, जलसे और जलूस निकलने लगे। अमृतसर में अंग्रेजी सरकार ने डॉन सतपाल और डॉन किचलू को पकड़ लिया। कोई 20,000 लोगों ने इसके विरोध में 13 अप्रैल, 1919 ई. को जलियाँवाला बाग (Jallianwala Bagh) में एक जलसा किया। शीघ्र ही एक अंग्रेज़ अधिकारी जनरल डायर (General Dyer) ने बाग को चारों ओर से घेर लिया और गोली चलाना प्रारम्भ कर दिया जिससे सहस्त्रों स्त्री-पुरुष मारे गये और अनेकों घायल हुए। इस हत्याकाण्ड का भारतीय राजनीति पर प्रभाव-जलियाँवाला बाग के हत्याकांड ने भारतीयों पर बड़ा गहरा प्रभाव डाला। अब लोगो का अंग्रेजी शासन से विश्वास जाता रहा और वे ऐसे शासन से छुटकारा पाने के लिए उग्र और क्रान्तिकारी मार्ग पर चल पड़े। सरकार ने भी अपना दमन-चक्र और तेज कर दिया।
सारे पंजाब में मार्शल-ला (Martial Law) लगा दिया और बड़े अत्याचार किए। महात्मा गाँधी को भी कैद कर लिया गया। जेल से आते ही उन्होंने पंजाब के हत्याकाण्ड और मार्शल-ला के विरुद्ध खिलाफत आन्दोलन चलाया हुआ था, को अपने साथ मिलाकर 1920 ई. में पहला असहयोग आन्दोलन चलाया। उनके कहने पर हजारों व्यक्तियों ने सरकारी नौकरियाँ छोड़ दी और सरकार से मिले हुए पदक और उपाधियाँ त्याग दी। वकीलों ने वकालत छोड़ दी और विद्यार्थियों ने अपने स्कूल तथा कॉलिज छोड़ दिए। इस प्रकार हम कह सकते है कि जलियाँवाला बाग के हत्याकाण्ड की घटना भारत के इतिहास में अपना विशेष महत्व रखती है। इसके परिणामस्वरूप जहाँ एक ओर अंग्रेजी सरकार के नैतिक सम्मान और गौरव को धक्का लगा, वहाँ जनता और सरकार के अच्छे सम्बन्ध सदा के लिए खराब हो गए। इस घटना से राष्ट्रीय एकता और सुदृढं हुई जब सभी जातियों के लोग सरकार के अत्याचारों के सम्मान रूप से शिकार हुए। परन्तु जब सरकार की दमनकारी नीति भारतीयों को भयभीत करने में असफल रही तो निश्चित रूप से भारतीयों का धैर्य और मनोबल कई गुना बढ़ गया और वे अधिक शक्ति से भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम में जुट गए।
(ख) साइमन कमीशन
उत्तर-
असहयोग आन्दोलन के वापस लेने के पश्चात् जब प्रसिद्ध नेता सी.आर.दास (C.R.Dass) की मृत्यु हो गई तो देश में एक प्रकार का सन्नाटा छा गया। केवल क्रान्तिकारी ही इधर-उधर अपना क्रान्तिकारी कार्य करते रहे। इस रातनीतिक सन्नाटे को तोड़ने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1927 ईन में जॉन साइमन (John Simon) की अध्यक्षकता में एक कमीशन नियुक्त किया जिसके मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित थे:
(क) इसका मुख्य उद्देश्य तो यह था कि 1919 के गर्वनमेंट आफ इण्डिया ऐक्ट की समीक्षा की जा सके ताकि यह सुझाव दिए जा सके कि भारतीय प्रशासन में क्या नए सुधार लाए जा सकते हैं।
(ख) इसका एक अन्य उद्देश्य यह भी था कि भारत में पैदा तत्कालीन राजनीतिक सन्नाटे और गतिरोध को दूर किया जा सके। क्योंकि इस कमीशन का अध्यक्ष जॉन साइमन को बनाया गया इसलिए साधारणतया इसे साइमन कमीशन के नाम से पुकारा जाता है।
साइमन कमीशन में सात सदस्य थे और वे सबके सब अंग्रेज थे। इसलिए जब यह कमीशन 1928 ई. में भारत आया तो सभी स्थानों पर लोगों ने इसका बहिष्कार किया। जहाँ भी यह कमीशन जाता था वहाँ हड़ताले होती थीं, काली झण्डियाँ दिखाई जाती थीं और ‘साइमन लौट जाओ’ (Simon Go Back) के नारे लगाए जाते थे।
साइमन का बहिष्कार क्यों किया गया? अब प्रशन यह है कि इस साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया। इसके कारणों को ढूँढना कोई कठिन नही:
(1) इस कमीशन के बहिष्कार का पहला कारण यह था कि इसका कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था। लोगों का विश्वास था कि भारत के विषय में कोई भी कमीशन ठीक नहीं सोच सकता जब तक उसमें कोई भी भारतीय सदस्य न हो।
(2) दूसरे, इस कमीशन की धाराओं में भारतीयों को स्वराज दिए जाने की कोई भी सम्भावना नहीं थी।
(3) तीसरे, जब भारतीयों ने इस बात की मांग की कि इस कमीशन में कोई भारतीय सदस्य भी होना चाहिए क्योंकि एक भारतीय ही उनकी समस्याओं को भली-भाँति समझ सकता है। भारतीयों का कहना था कि ब्रिटेन के ‘हाउस आफ कॉमस’ (House of Commons) के किसी भारतीय सदस्य, विशेषकर श्री एस.पी.सिन्हा (S.P.Sinha) का कमीशन में सम्मिलित कर लिया जाए ब्रिटिश सरकार ने इस मांग को भी अस्वीकृत कर दिया। इससे भारतीय उत्तेजित हो उठे।
(4) चौथा, अन्त में यह कहा जाता है कि यह मामला इतना तूल न पकड़ता यदि भारत सचिव लार्ड बैकन हैड (Lord Birken Head) भारतीयों का यह कह कर अपमान किया होता कि भारतीय लोग न तो संवैधानिक मामलों पर विचार विमर्श करने की क्षमता रखते है और न ही वे कोई एक ऐसे ढाँचे की रूप-रेखा प्रस्तुत कर सकते हैं जो सभी लोगों को मान्य हो।
प्रश्न. 4
इस अमयाय में दी गई भारत माता की छवि और अध्याय 1 में दी गई जर्मेनिया की छवि की तुलना कीजिए।
उत्तर-
विश्व भर में कलाकारों की यह प्रवृति रही है कि वे स्वतन्त्रता न्याय, गणतन्त्र आदि विचारों की व्यक्त करने के लिए नारी रूपक का प्रयोग करते हैं। उन्होने राष्ट्र को भी नारी रूप में प्रस्तुत किया। 1848 ई. में जर्मन चित्रकार फिलिप वेट (Philip Veit) ने अपने राष्ट्र को पन्नों को जर्मेनिया के रुप में प्रस्तुत किया। वे बलूत वृक्ष के पनों का मुकुट पहने दिखाई गई हैं क्योंकि जर्मन बलूत वीरता का प्रतीक है। भारत में भी अबनिंद्रनाथ टैगोर अनेक कलाकारों ने भारत राष्ट्र को भारत माता के रूप में दिखाया। एक चित्र में उन्होंने भारत माता के शिक्षा, भोजन और कपड़े देती हुई दिखाया हैं। शिक्षा’, भोजन और कपड़े दे रही है।
![]()